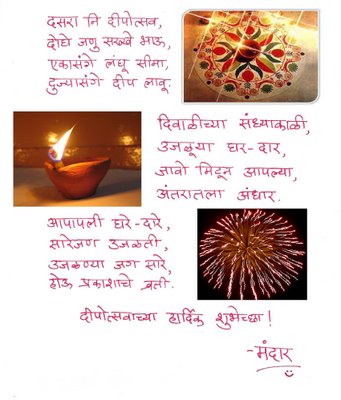ना लिख पाऊंगा हर्फ़-ए-इश्क तुझको मैं कभी,
सोचा लिख देता हूं कोई एक ग़ज़ल ही सही
तेरा साथ ना हुआ हासिल तेरी यादें ही सही,
तेरा हाथ न है हाथ में, तेरा एहसास ही सही
बारिश की राह तकती आंख में भर गये आंसूं,
गूंजते बादलों के साथ वो अकेली शाम ही सही
क्या बात अगर तुझे कभी पा न सकूंगा मैं
तेरे आशिकों कि शुमार में मेरा नाम ही सही
आंखें न देख सकती तुझे, न ये कान सुनते हैं,
"तू है, यहीं कहीं" दिल में ये एक खयाल ही सही
माना मेरे नसीब में नही है तेरे लब का जाम
तेरी जुबां पे उस रोज आया हुआ मेरा नाम ही सही
न बन सका तेरा आशिक, तेरा मजनू, तेरा बालम
तेरे चाहनेवालों में से मैं एक कोई 'बेनाम' ही सही
Sunday, October 29, 2006
मीर आणि काफ़िर
एका शांतशा संध्याकाळी, जगजित सिंगांच्या आवाजातली माझी एक आवडती ग़ज़ल ऐकत होतो.
"पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं
जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं"
...अप्रतिम !
ही ग़ज़ल लिहिली होती मीर तकी मीर यांनी. 18 व्या शतकातले मोठे शायर. मिर्झा़ असदुल्लां खां गा़लिब सारख्यांनी मीर यांच्या शायरीचा आदराने उल्लेख केला आहे, मीर यांना उर्दू शायरीचे 'ईमाम' मानून. गुलजारनी बनवलेल्या "मिर्झा गा़लिब" या दूरदर्शनवरच्या मालिकेत तसा एक प्रसंगही दाखवला आहे. मीर यांचा हा शेर ऐकून गा़लिब उद्गारले होते:
"रेख्ते के तुम ही एक उस्ताद नही हो गा़लिब,
कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था"
मीर यांचा आणखी एक शेर वाचला काही दिवसांपूर्वी :
"सख्त काफ़िर था जिसने पहले 'मीर',
मज़हब-ए-इश्क़ इख़्तियार किया .. "
'काफ़िर'या कल्पनेवर विचार करताना माझ्या मनात आलं,
"पथ्थर के बूतों के दीवाने होते हैं काफ़िर,
ना बूतों में जान हैं ना जिगरवाले हैं काफ़िर"
आणि, मजहब-ए-इश्क यावरच बोलायचं झालं तर,
"फ़र्क न है मजहब-ए-इश्क में मालिक-बन्दे का,
गो कत्ल करता है मालिक, सीने से भी लगाता है"
"पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं
जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं"
...अप्रतिम !
ही ग़ज़ल लिहिली होती मीर तकी मीर यांनी. 18 व्या शतकातले मोठे शायर. मिर्झा़ असदुल्लां खां गा़लिब सारख्यांनी मीर यांच्या शायरीचा आदराने उल्लेख केला आहे, मीर यांना उर्दू शायरीचे 'ईमाम' मानून. गुलजारनी बनवलेल्या "मिर्झा गा़लिब" या दूरदर्शनवरच्या मालिकेत तसा एक प्रसंगही दाखवला आहे. मीर यांचा हा शेर ऐकून गा़लिब उद्गारले होते:
"रेख्ते के तुम ही एक उस्ताद नही हो गा़लिब,
कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था"
मीर यांचा आणखी एक शेर वाचला काही दिवसांपूर्वी :
"सख्त काफ़िर था जिसने पहले 'मीर',
मज़हब-ए-इश्क़ इख़्तियार किया .. "
'काफ़िर'या कल्पनेवर विचार करताना माझ्या मनात आलं,
"पथ्थर के बूतों के दीवाने होते हैं काफ़िर,
ना बूतों में जान हैं ना जिगरवाले हैं काफ़िर"
आणि, मजहब-ए-इश्क यावरच बोलायचं झालं तर,
"फ़र्क न है मजहब-ए-इश्क में मालिक-बन्दे का,
गो कत्ल करता है मालिक, सीने से भी लगाता है"
Thursday, October 19, 2006
Subscribe to:
Comments (Atom)